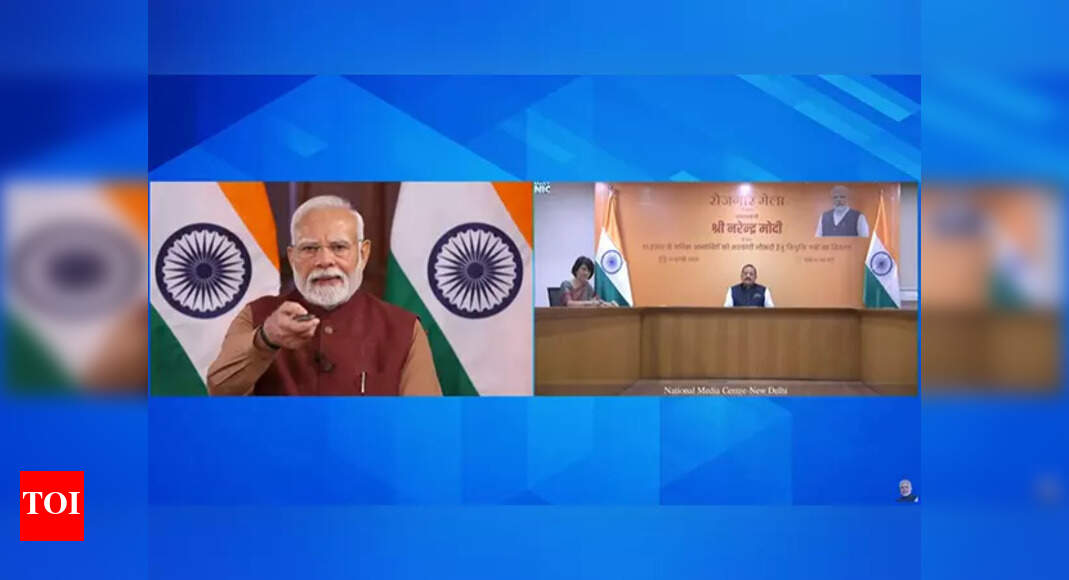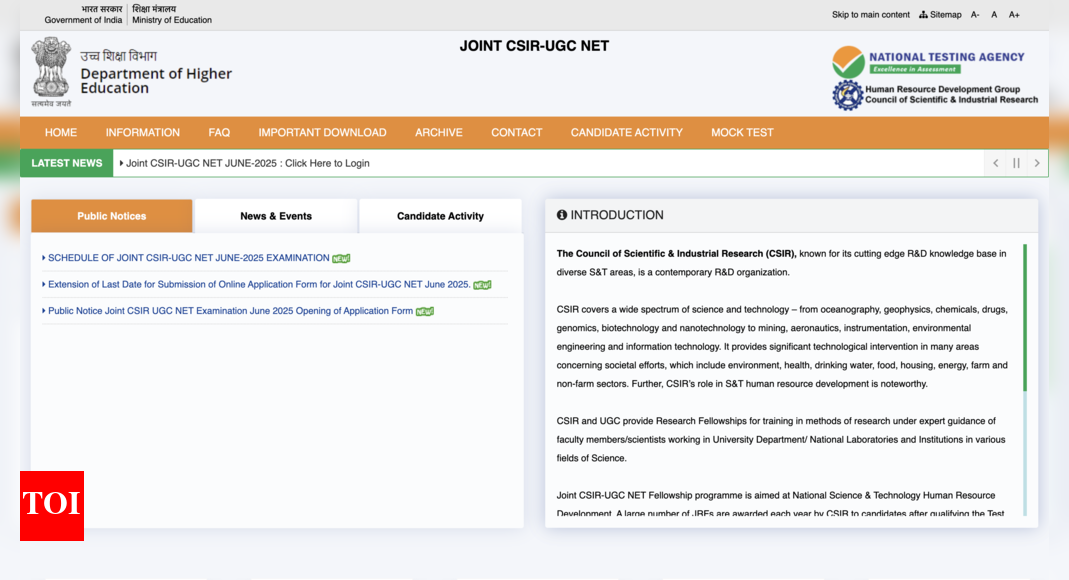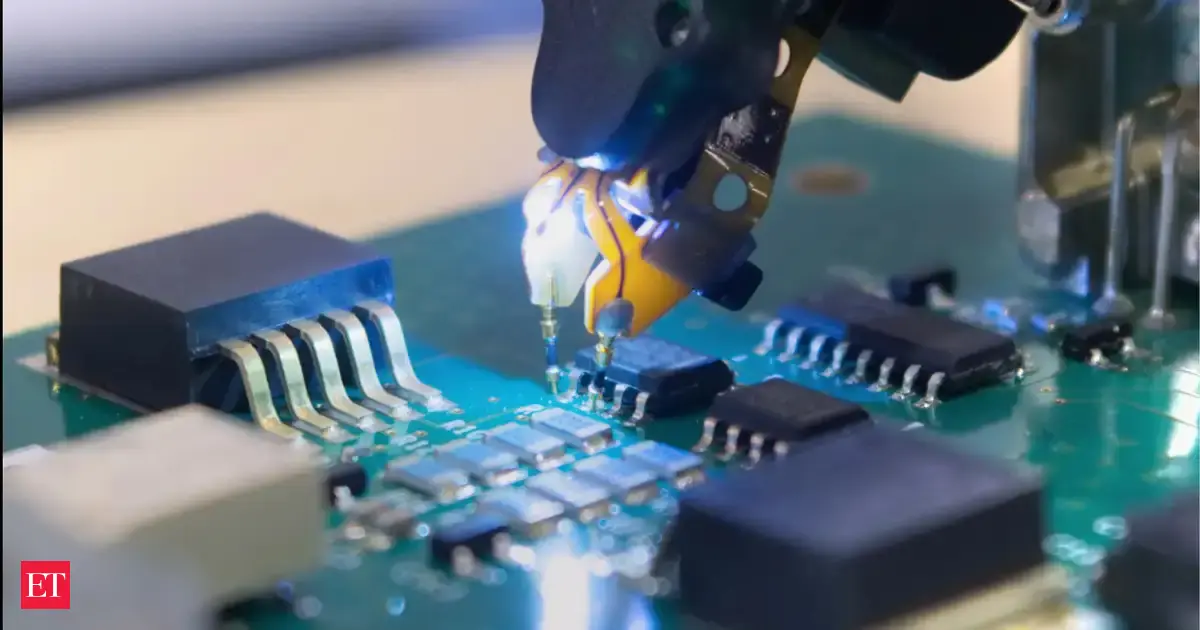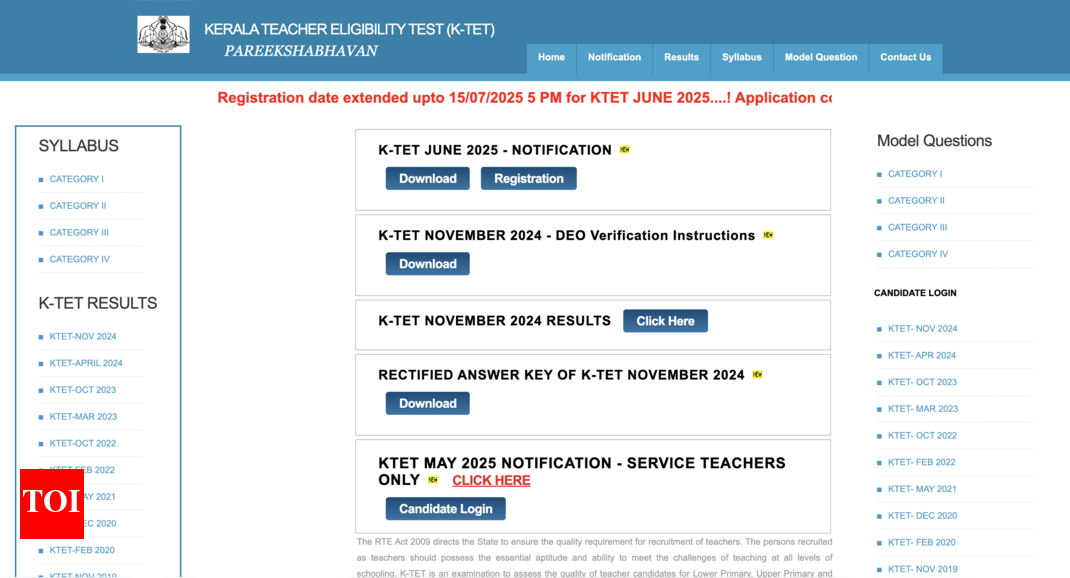विशेषज्ञों के मुताबिक, व्यूअरशिप मापने वाली प्रणाली चलाना एक पूंजी-सघन प्रक्रिया है, जिसमें हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश लगता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण बाजार में कई एजेंसियों का संचालन संसाधनों को और अधिक विभाजित कर सकता है, जिससे डेटा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। एडवरटाइजिंग जगत के वरिष्ठ विशेषज्ञ आशिष भसीन ने चेताया कि भारत अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा,”हम पहले भी TAM और INTAM के जमाने में इस भ्रम को देख चुके हैं। इससे कोई लाभ नहीं हुआ। भारत जैसे बहुभाषी और विविध उपभोग वाले बाजार में एक मजबूत और भरोसेमंद रेटिंग फ्रेमवर्क ही कारगर हो सकता है।”
ताक़तवर खिलाड़ियों को बढ़त ?
विश्लेषकों ने यह भी चिंता जताई है कि ज्यादा संसाधनों वाले खिलाड़ी, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स या बड़े मीडिया घराने, इस मौके का फायदा उठाकर रेटिंग प्रणाली पर प्रभाव डाल सकते हैं। इससे पूरी प्रणाली में पावर इम्बैलेंस पैदा हो सकता है।
सुधार ज़रूरी, लेकिन संतुलन बना रहे
उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि सुधारों की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए मौजूदा प्रणाली को तोड़ने की बजाय मजबूत करना ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न समितियों ने सैंपलिंग, गवर्नेंस और मेथडोलॉजी जैसे पहलुओं में सुधार की सिफारिशें की हैं, जिन्हें अब लागू करने की ज़रूरत है। सरकार की यह नीति बदलाव लाने की मंशा तो रखती है, लेकिन इसके वास्तविक क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। यदि इस प्रक्रिया में डेटा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तो यह प्रयोग उद्योग में भ्रम और असंतुलन की वजह भी बन सकता है।